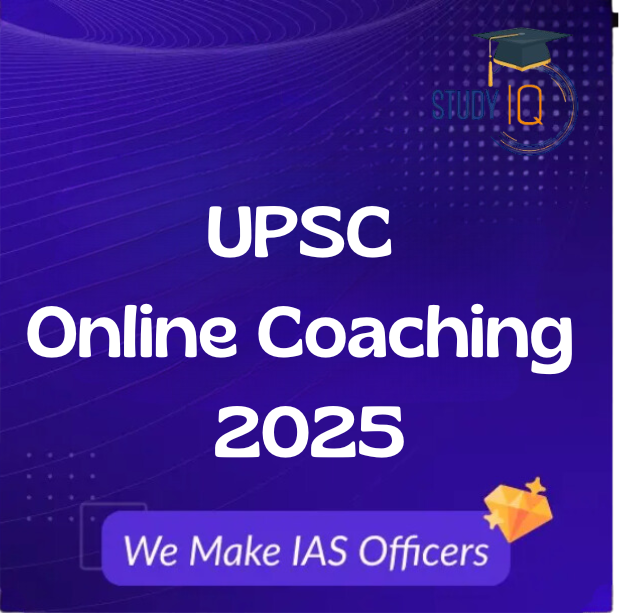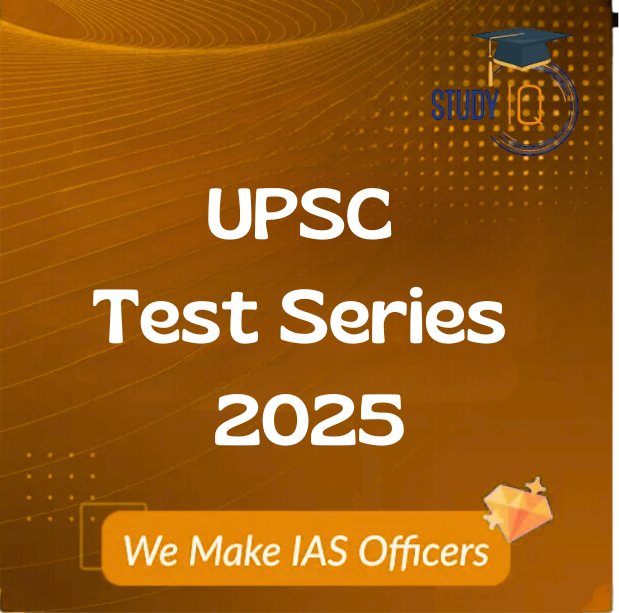Table of Contents
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए ‘न्यायाधीशों के स्थानांतरण‘ के मुद्दे की प्रासंगिकता
न्यायाधीशों का स्थानांतरण: न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मुद्दे में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र: न्यायपालिका एवं भारतीय संविधान सम्मिलित है।
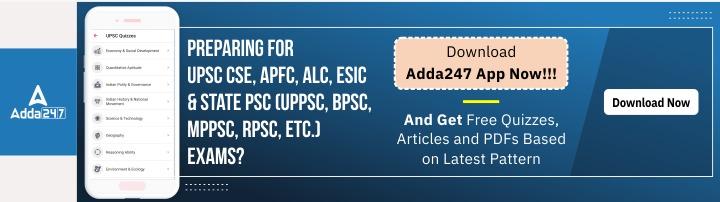
न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मुद्दा चर्चा में क्यों है?
अधिवक्ताओं ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया/सीजेआई) को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (जस्टिस करियल) के स्थानांतरण का मामला उठाया, अफवाहों का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आसन्न स्थानांतरण के बारे में अनभिज्ञ थे।
न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर संवैधानिक प्रावधान
- संविधान का अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है एवं कहता है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श के पश्चात, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- यह अनुच्छेद व्यापक न्यायिक समीक्षा एवं व्याख्या के अधीन रहा है तथा ऐतिहासिक संदर्भ के प्रत्याह्वान से इसके वर्तमान उपयोग एवं रूपरेखा को समझने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन क्या है?
- प्रक्रिया ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) इस संदर्भ में स्पष्ट है कि स्थानांतरण हेतु न्यायाधीश की सहमति आवश्यक नहीं है।
- वर्तमान मानदंड यह है कि सभी स्थानान्तरण जनहित में, अर्थात संपूर्ण देश में न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होने चाहिए।
- इसमें यह भी कहा गया है कि न्यायाधीश के व्यक्तिगत कारकों, जिसमें उनके स्थान की वरीयता भी शामिल है, को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- यह कोई नहीं जानता कि ये आवश्यकताएं प्रत्येक मामले में पूरी होती हैं अथवा नहीं।
न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय
संकलचंद एच शेठ का वाद
- 1970 का दशक भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में अनेक न्यायाधीशों के अधिक्रमण एवं उच्च न्यायालय के अनेक न्यायाधीशों का स्थानांतरण का भी साक्षी बना।
- आपातकाल के पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने संकलचंद एच सेठ के वाद में अनुच्छेद 222 की व्याख्या की।
- बहुमत से सहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने कहा कि एक न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण व्यक्ति को अनेक क्षति पहुंचाता है।
- उन्होंने कहा कि स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश की सहमति अनुच्छेद 222 की योजना एवं भाषा का हिस्सा थी।
- उन्होंने यह भी माना कि यदि स्थानांतरण की शक्ति पूर्ण रूप से कार्यपालिका के पास निहित है, तो यह न्यायिक स्वतंत्रता को दुर्बल करती है एवं संविधान की मूल विशेषताओं को नष्ट कर देती है।
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय न्यायाधीशों के वाद
- इन तीन मामलों ने अनुच्छेद 222 एवं उसके कार्यकरण की व्याख्या की।
- संचयी रूप से, न्यायाधीशों के पहले एवं दूसरे वाद के परिणामस्वरूप भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ “परामर्श” की व्याख्या करके वास्तव में “सहमति“ की व्याख्या करके कॉलेजियम प्रणाली का गठन किया गया।
- इस तरह की सहमति एक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की है एवं दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ चर्चा करने के उपरांत मुख्य न्यायाधीश द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है।
- न्यायाधीशों के तृतीय वाद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों को सम्मिलित करने के लिए कॉलेजियम का विस्तार किया।
के. अशोक रेड्डी वाद
- 1994 में, न्यायाधीशों के द्वितीय एवं तृतीय वाद के मध्य, के. अशोक रेड्डी का वाद सर्वोच्च न्यायालय में विशेष रूप से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के प्रश्न से निपटने के लिए दायर किया गया था।
- इसमें उठाया गया तर्क यह था कि इस तरह के स्थानांतरण “असंबद्ध विचारों से प्रभावित होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप स्वेच्छाचारिता होती है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्षरण होता है”।
- इस वाद में यह भी कहा गया कि “संपूर्ण देश में न्याय के बेहतर प्रशासन” को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग केवल “सार्वजनिक हित” में किया जा सकता है।
क्या के. अशोक रेड्डी वाद में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों की फिर से जांच करने का समय आ गया है?
- संकलचंद सेठ वाद में 44 वर्ष पूर्व न्यायमूर्ति भगवती द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जो विचार रखा गया था, वह संभवतः आज के समय में अधिक प्रयोज्यता के साथ उचित था।
- यदि स्थानान्तरण “जनहित“ पर आधारित हैं तो जनता को ऐसे कारणों को जानने का अधिकार है।
- यह ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिस पर न्यायाधीश के स्थानांतरण से पूर्व अथवा जब न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर विचार किया जा रहा हो, संबंधित न्यायाधीश एवं समस्त हितधारकों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- कोई भी यह समझ सकता है कि कभी-कभी यह सामग्री न्यायाधीश को असमंजस में डाल सकती है। किंतु एक संतुलन अवश्य बनाया जा सकता है।
- जब स्थानांतरण के कारण अज्ञात हैं, तो यह अटकलें लगाई जाती हैं कि केवल “असुविधाजनक“ न्यायाधीशों का ही स्थानांतरण होता है।
आगे क्या?
- देश भर में प्रतिभाओं के आदान-प्रदान एवं न्यायपालिका में स्थानीय गुटों को उभरने से रोकने के लिए न्यायाधीशों के स्थानांतरण की आवश्यकता हो सकती है।
- यद्यपि, हस्तांतरण की शक्ति को सदैव न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखा गया है।
- कोई अच्छा संदेश नहीं भेजा जा रहा है यदि यह माना जाता है कि कॉलेजियम अधिवक्ताओं के एक समूह द्वारा की गई मांग पर ध्यान देता है, किंतु दूसरे समूह की उपेक्षा करता है।
- कॉलेजियम प्रणाली के तहत भी, इस धारणा को दूर करना कठिन प्रतीत होता है कि प्रत्येक न्यायाधीश के सिर पर स्थानांतरण का खतरा मंडराता रहता है। जैसा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संदर्भ में प्रक्रिया ज्ञापन स्पष्ट है कि स्थानांतरण को प्रभावित करने के लिए न्यायाधीश की सहमति आवश्यक नहीं है।
- इस स्थिति में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के प्रावधानों की पूर्ण समीक्षा का समय संभवतः आ गया है।
निष्कर्ष
जब न्यायपालिका आधारिक संरचना के सिद्धांत को बनाए रखने एवं किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का कोई अवसर नहीं चूकती है, तो पक्षपात, पूर्वाग्रह अथवा सरकारी हस्तक्षेप की सभी धारणाओं को दूर करने के लिए न्यायिक कामकाज में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। यह न केवल “लोक हित” में है बल्कि न्यायिक संस्थान के व्यापक कल्याण के लिए भी है।
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मुद्दे से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?
उत्तर. संविधान का अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है एवं कहता है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया/CJI) से परामर्श के पश्चात, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं।
प्र. किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करने से पूर्व सहमति के बारे में मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) क्या कहता है?
उत्तर. न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन स्पष्ट है कि स्थानांतरण को क्रियान्वित करने के लिए न्यायाधीश की सहमति आवश्यक नहीं है।

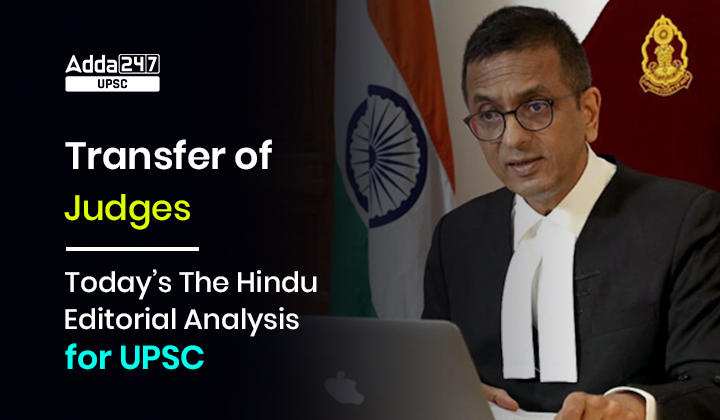

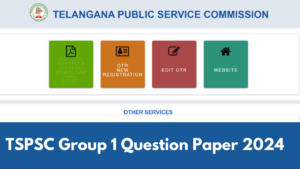 TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...
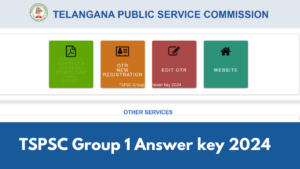 TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...
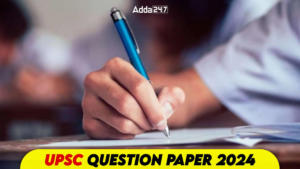 UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...
UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...